हम कैसे काम करते हैं
वायरल, हानिकारक खबरों की जांच
एएफ़पी के फ़ैक्ट चेक रिपोर्टर ऑनलाइन शेयर की गयी उन वायरल संदिग्ध दावों की जांच करते हैं जो संभावित रूप से जनता के लिए हानिकारक हो सकते हैं. हम सोशल मीडिया, ब्लॉग, वेबसाइट, मैसेजिंग ऐप्स और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य प्लेटफ़ॉर्म सहित विभिन्न तरीकों से शेयर किये गये दावों की पुष्टि और सत्यापन करते हैं.
हम दावों को ये ध्यान में रखते हुए चुनते हैं कि क्या यह फ़ैक्ट-चेक सार्वजनिक हित में है और क्या हम इस दावे या किए जा रहे दावों को खारिज करने या भ्रामक बताने के लिए स्पष्ट और पर्याप्त साक्ष्य एकत्र करने में सक्षम होंगे. एएफ़पी की फ़ैक्ट-चेक टीमें सिर्फ़ तथ्यों की पुष्टि करती हैं, किसी भी तरह की राय या आस्था की नहीं. अगर हम किसी फ़ैक्ट चेक रिपोर्ट में पुख़्ता साबुत और तथ्य नहीं जुटा पाए तो हम उस फ़ैक्ट-चेक को प्रकाशित नहीं करेंगे.
हम उन गलत सूचनाओं पर विशेष ध्यान देते हैं जो लोगों के स्वास्थ्य या जीवन को खतरे में डाल सकती हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं, या अभद्र भाषा (हेट स्पीच) और नस्लवाद को बढ़ावा दे सकती हैं.
भले ही दावा किसी ने भी किया हो, हम अपने फ़ैक्ट चेक में एक खोजी दृष्टिकोण और साक्ष्य/तथ्य के मानकों को लागू करते हैं. हम किसी एक उम्मीदवार, पार्टी या वेबसाइट पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं. हालांकि हम उन स्रोतों या अकाउंट्स को फ़ैक्ट चेक करने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं जो लगातार संभवतः हानिकारक या गलत सूचना फैलाते हैं. वे नैतिक मानक जो एएफ़पी की निष्पक्षता और स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता को कायम रखते हैं, उनके बारे में आप यहां और पढ़ सकते हैं.
सार्वजनिक स्रोत (ओपन सोर्स)
हमारे फ़ैक्ट-चेक गैर-पक्षपातपूर्ण और हमारे रिपोर्टर्स द्वारा एकत्रित की गई प्राथमिक स्रोत सामग्री पर आधारित होते हैं, जिसमें एएफ़पी के स्वयं के आर्काइव के माध्यम से सत्यापित सामग्री और दुनिया भर में एजेंसी के ग्राउंड रिपोर्टर्स के सहयोग से इकठ्ठा की गई सूचना सामग्री शामिल है. हम विशेषज्ञों से भी बात करते हैं और अपने फ़ैक्ट-चेक में उन्हें शामिल भी करते हैं, यह ध्यान में रखते हुए कि वे किसके लिए काम करते हैं, उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र क्या है और हितों के टकराव की कोई सम्भावना है या नहीं. किसी भी फ़ैक्ट-चेक के मुख्य दावे को वेरीफ़ाई करने के लिए हमें कम-से-कम दो स्वतंत्र सूचना-स्नोतों की आवश्यकता होती है.
किसी भी फ़ैक्ट चेक में इस्तेमाल किये गए तमाम तरीके हम बिलकुल पारदर्शिता के साथ दिखाने की कोशिश करते हैं. इसके लिए हम अपने रिपोर्ट्स में उन सभी लिंक्स, एम्बेड, स्क्रीनशॉट, फ़ोटो और इकठ्ठा किये गये अन्य सबूतों को शामिल करते हैं जो हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करते हैं. हमारा लक्ष्य पाठकों को यह समझाना है कि कोेई भी फ़ैक्ट-चेक जांच कैसे की गई है और वो स्वयं उन्हीं स्टेप्स को अपना कर कोई फ़ैक्ट-चेक कैसे कर सकते हैं.
सामान्यतः एएफ़पी अपने फ़ैक्ट-चेक में अनाम या अज्ञात स्रोतों का उपयोग नहीं करता है. ऐसा किसी असाधारण मामले में ही हो सकता है जहां किसी स्रोत की सुरक्षा खतरे में हो और उसके द्वारा प्रदान की गई जानकारी फ़ैक्ट चेकिंग के लिए आवश्यक भी हो और अन्य सार्वजनिक स्रोतों द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई हो.
यदि जांच के दौरान किसी दावे का कोई हिस्सा हम सत्य पाते है, तो अपने फ़ैक्ट-चेक में इसे स्वीकार भी करते हैं.
दावे की जांच के लिये टूल और हमारा दृष्टिकोण
हम किसी भी दावे की जांच के लिये पत्रकारिता कौशल और कई साधारण टूल्स, कुछ सामान्य ज्ञान और बेहद धैर्य और सावधानी का उपयोग करते हैं.
उदाहरण के लिए, यदि हमें लगता है कि किसी तस्वीर को मॉर्फ़ या एडिट किया गया है या उसे संदर्भ से अलग शेयर किया गया है, तो हम सबसे पहले मूल तस्वीर की खोज करते हैं और इसके बारे में अधिक जानने के लिए फ़ोटोग्राफ़र या संबंधित सोर्स से बात करने का प्रयास करते हैं. यदि हम किसी ऐसे दावे की जांच कर रहे हैं जो किसी तर्क के समर्थन में डाटा प्रस्तुत करता है, तो हम मूल स्रोत की खोज करेंगे और उस दावे में दिये गये आंकड़ों के बारे में विशेषज्ञों से उनकी राय जानने के लिए बात करेंगे.
गलत जानकारी की पोस्ट पर बढ़ते क्लिक से बचने के लिए और बाद में किसी पोस्ट के एडिट होने या डिलीट होने की स्थिति में रिकॉर्ड रखने के लिए हम वेबैक मशीन या पर्मा सीसी जैसे कई अन्य आर्काइव टूल्स का उपयोग करते हैं. नीचे उन तरीकों का एक खाका दिया गया है जिनका हम नियमित रूप से अपने डिबंक/फ़ैक्ट-चेक में उपयोग करते हैं:
नीचे उन तरीकों का एक खाका दिया गया है जिनका हम नियमित रूप से अपने डिबंक/फ़ैक्ट-चेक में उपयोग करते हैं:
तस्वीरों की जांच
बहुत सी गलत सूचनाओं में ‘संदर्भ से बाहर’ प्रयोग की गई पुरानी तस्वीरें शामिल होती हैं.
किसी भी तस्वीर के स्रोत का पता लगाने के लिए या यह पता लगाने के लिये कि क्या वह पहले से ऑनलाइन कहीं मौजूद है, हम एक या कई सर्च इंजनों में तस्वीर को अपलोड करके रिवर्स इमेज सर्च से शुरू करते हैं.
गूगल क्रोम ब्राउज़र (Google Chrome) पर किसी तस्वीर पर राइट क्लिक करने से "तस्वीर को गूगल पर खोजें" नाम से एक विकल्प मिलता है. सर्च इंजन अपने डेटाबेस में यह देखता है कि क्या इससे मिलते जुलते चित्र उसके सूचकांक में मौजूद हैं.
हम अपनी जांच में InVID/WeVerify एक्सटेंशन का भी नियमित रूप से उपयोग करते हैं, जो आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद किसी तस्वीर पर एक साधारण राइट क्लिक के साथ Google, Bing, Yandex, TinEye और Baidu सहित कई इमेज सर्च इंजन का विकल्प उपलब्ध कराता है.
यह ध्यान रखें कि रिवर्स सर्च हमेशा सही और संतोषजनक परिणाम नहीं देता है क्योंकि या तो खोजी गई तस्वीर इंटरनेट पर कभी प्रकाशित नहीं हुई है या फिर उसे अभी तक अनुक्रमित नहीं किया गया है. कभी-कभी रिवर्स इमेज सर्च इंजन किसी ऐसी इमेज से भ्रमित हो सकते हैं, जिसे फ़्लिप किया गया है, जैसे कि एक पूर्व जापानी प्रधानमंत्री के बारे में सर्च करते हुए इस स्टोरी में हमारे साथ ऐसा हुआ.
किसी भी तस्वीर के स्थान या तिथि का पता लगाने के लिए हम दृश्य संकेतों (जैसे दुकान के संकेत, सड़क के संकेत, वास्तुकला डिज़ाइन, पेड़ पौधे, लाइसेंस प्लेट) का भी बहुत ध्यान से निरीक्षण करते हैं.
उदाहरण के लिए, जैसा नीचे दिखाया गया है, इस पड़ताल में एक वीडियो में दिखाए गए स्थान की पुष्टि करने के लिए पहले एएफ़पी ने इसमें दिख रही एक बिल्डिंग की पहचान की और फिर गूगल स्ट्रीट व्यू के साथ इसकी तुलना करके फ़ैक्ट चेक को पूरा किया.
नीचे हमने वीडियो में दिख रहे एम्स्टर्डम स्थित मैडम तुसाद संग्रहालय के बोर्ड की क्लिप में दिख रही तस्वीर (बाएं) और उसी स्थान पर देखी गई एक गूगल स्ट्रीट व्यू तस्वीर (दाएं) की स्क्रीनशॉट की तुलना की है:

सिर्फ़ फ़ोटो या वीडियो आमतौर पर किसी भी दावे को सत्यापित करने के लिये पर्याप्त प्रमाण नहीं होते हैं. हमें उस तस्वीर की और जांच करने की भी आवश्यकता है, जैसे कि उसके प्रकाशित होने की तिथि और इसके भीतर के अन्य विवरण, जैसे कि उस समय मौसम की स्थिति आदि.
किसी भी संदिग्ध तस्वीर पर काम करते समय यह पता लगाने के लिए कि क्या उसे एडिट किया गया है, हम हमेशा मूल फ़ाइलों को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करते हैं.
वीडियो की जांच कैसै करें
वीडियो का विश्लेषण करने के लिए हम InVID/WeVerify एक्सटेंशन का भी उपयोग करते हैं, जिसे एएफ़पी द्वारा सह-विकसित किया गया है. यह टूल हमें किसी भी वीडियो को थंबनेल में काटने और फिर उन्ही तस्वीरों पर कई रिवर्स सर्च करने की सुविधा देता है.
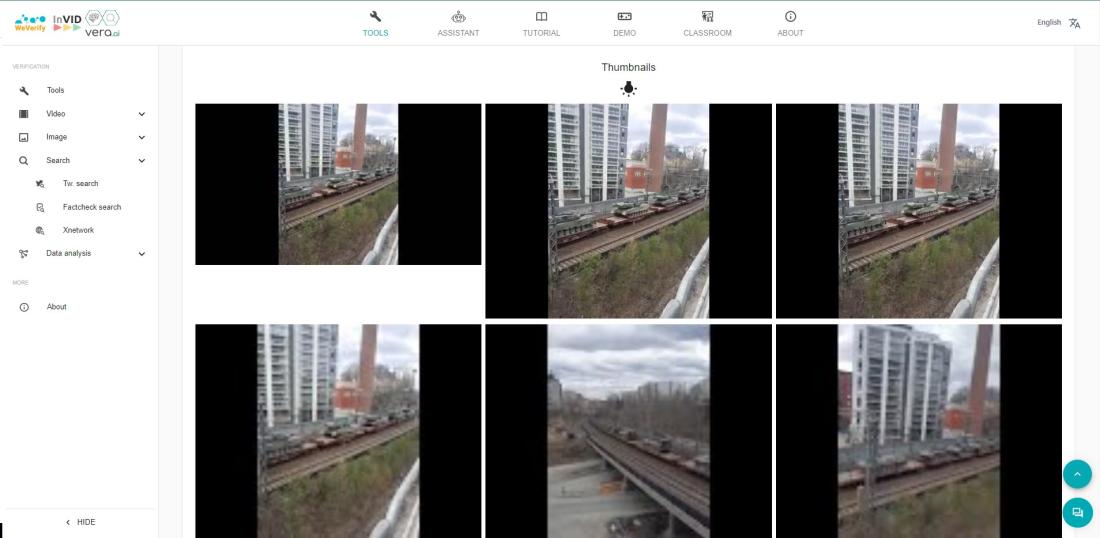
यदि आपको लगता है कि एक तस्वीर फ़्लिप की गई है तो यह एक्सटेंशन आपको इसे वापस फ़्लिप करने की सुविधा देता है.
कमेंट्स और डेटा को खोजना और सत्यापित करना
किसी सर्च इंजन में किसी टेक्स्ट के एक पैराग्राफ़ को साधारण कॉपी-पेस्ट करके अक्सर इसके स्रोत का पता लगाया जा सकता है, अगर यह पहले ही ऑनलाइन कहीं प्रकाशित हो चुका है.
यदि किसी कमेंट का श्रेय किसी व्यक्ति को दिया जाता है, तो हम उससे जुड़े किसी विश्वसनीय स्रोत (ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग, आधिकारिक लेख) की तलाश करते हैं. साथ ही आगे के सत्यापन के लिए उस व्यक्ति के ऑनलाइन अकाउंट्स को चेक हैं. कई बार हम बयान की पुष्टि करने के लिए सीधे उस व्यक्ति से भी संपर्क करते हैं.
मात्रात्मक डेटा को चेक करते समय हम पूरी तरह से इसका मूल अध्ययन और इसकी कार्यप्रणाली (Methodology) की तलाश करते हैं और उन विशेषज्ञों से बात करते हैं जो या तो मूल स्टडी के लेखक हैं या फिर कोई विशेषज्ञ जिसके पास उसी क्षेत्र में रिसर्च के अनुभव के साथ यह सत्यापित करने के पर्याप्त साक्ष्य हों कि क्या डेटा को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है.
हम नियमित रूप से उन विषयों से भी निपटते हैं जिनके बारे में हमें पहले से अधिक जानकारी नहीं होती है. इन मामलों में हम किसी विशिष्ट विषय, क्षेत्र या भाषा में विशेषज्ञता रखने वाले एएफ़पी के पत्रकारों से भी सहयोग लेते हैं. हम कई अन्य क्षेत्रों से संबंधित दावों के पहलुओं की जांच करने के लिए एएफ़पी की वैश्विक फ़ैक्ट-चेक टीम के साथ मिलकर काम करते हैं.
AI-जनरेटेड कंटेंट
हर नई तकनीक की तरह, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) नए उपकरण और नई चुनौतियां लेकर आया है.
AI से बनाए गए कंटेंट को वेरीफ़ाई करना अब पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, हालांकि हमारी ज़्यादातर जांच अभी भी ऐसी तकनीकों पर टिकी है जो कम जटिल तरीकों से गलत जानकारी को पहचान सकती है.
एएफ़पी के पास AI से बने कंटेंट को हैंडल करने के लिए आंतरिक दिशानिर्देश हैं. इस क्षेत्र में तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं, इसलिए इन गाइडलाइंस को समय-समय पर अपडेट किया जाता है. हम सिर्फ़ किसी AI-डिटेक्शन टूल की रिपोर्ट के आधार पर किसी कंटेंट को गलत नहीं कह सकते. हमें हमेशा दूसरी जांच भी करनी होती है, जैसे कि रिवर्स इमेज सर्च आदि. AI से हम किस प्रकार डील करते हैं, इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी AFP की एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज़ और फ़ैक्ट-चेकिंग स्टाइलबुक में दी गई है.
जानकारी को क्रॉस चेक करना
यदि इंटरनेट पर प्रसारित होने वाला कोई भी दावा संदिग्ध लगता है - विशेष रूप से यदि वह किसी भरोसेमंद स्रोत का हवाला नहीं देता है - तो हमारी पहली प्रतिक्रियाओं में से एक उसके कमेंट्स को पढ़ना होता है.
कमेंट्स में आमतौर पर कुछ न कुछ विरोधाभासी जानकारी मिल ही जाती है जिससे हमें कोई लीड अवश्य मिलती है या फिर कोई न कोई यूज़र दावे की सत्यता पर सवाल ज़रूर खड़ा करता है.
यदि कमेंट में किसी व्यक्ति या संगठन का उल्लेख किया जाता है, तो हम उस घटना से जुड़ा उनका वर्ज़न जानने के लिए उनसे संपर्क करते हैं. अगर उपयुक्त और संभव हो तो हम और जानकारी प्राप्त करने के लिए जांच के तहत उस दावे के स्रोत से भी संपर्क करते हैं.
यदि कोई संदिग्ध प्रकाशन किसी तस्वीर या वीडियो पर आधारित है, तो हम उनकी तुलना करने के लिए उसी घटना से जुड़ी अन्य तस्वीरों की खोज करते हैं और अधिक जानकारी के लिए तस्वीर के मूल फ़ोटोग्राफ़र या ओनर से भी संपर्क करते हैं.
सिर्फ़ इंटरनेट ही पर्याप्त नहीं
कुछ फ़ैक्ट-चेक रिपोर्ट्स के लिए सिर्फ़ इंटरनेट और टेलीफ़ोन ही पर्याप्त नहीं होते हैं. कभी कभी - जो कि पत्रकारिता का मूल है - आपको ग्राउंड पर रहने की आवश्यकता होती है. आमतौर पर जब किसी घटना या तथ्य को व्यक्तिगत रूप से सत्यापित किया जाना ज़रूरी हो तो हम अपने पत्रकारों को उन्हे व्यक्तिगत रूप से जाँच करने के लिए भेजते हैं. हम एएफ़पी के पत्रकारों के साथ भी मिलकर काम करते हैं जो दुनिया भर की खबरों को आन-द-ग्राउंड कवर कर रहे हैं.
उदाहरण के तौर पर, अप्रैल 2024 में एक लेख के लिए हमने एक वीडियो की जांच की, जिसमें कुछ सैन्य वाहन एक निर्माण स्थल के पास सड़क पर चलते हुए दिख रहे थे. वीडियो के कैप्शन में दावा किया गया था कि ये फ़्रेंच बख्तरबंद वाहन हैं, जो रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान यूक्रेन के ओडेसा शहर पहुंचे थे. हमने वीडियो की सच्चाई जांचने के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध ओपन-सोर्स जानकारियों का इस्तेमाल किया और यह पता लगाने की कोशिश की कि ये सैन्य वाहन किस देश के हो सकते हैं. इन टूल्स की मदद से हमने यह स्थापित किया कि वीडियो ओडेसा में नहीं, बल्कि पोलैंड में फ़िल्माया गया था. वीडियो में दिख रहे एक चुनावी पोस्टर की मदद से हम उस जगह को एक खास कस्बे तक सीमित कर पाए. इसके बाद, पोलैंड की राजधानी वॉरसॉ में स्थित एएफ़पी के ऑफ़िस ने उस कस्बे के स्थानीय अधिकारियों और चुनाव अभियान से जुड़े लोगों से संपर्क किया. उन्होंने हमें उस जगह की एक फ़ोटो दी जहां वीडियो फ़िल्माया गया था. इससे यह साफ़ हो गया कि वीडियो पोलैंड में शूट किया गया था, न कि ओडेसा में जैसा कि सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया था.
एडिटिंग और रेटिंग
फ़ैक्ट-चेक की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमारे पत्रकार क्षेत्रीय संपादकों के संपर्क में रहते हैं. संपादक पत्रकारों के साथ पोस्ट के दावों और उसके फ़ैक्ट-चेक पर चर्चा करते हैं, आकलन करते हैं और समझाते हैं कि अन्य किस तरह के तथ्यों की आवश्यकता होगी, और प्रकाशित होने से पहले आर्टिकल को एडिट करते हैं.
एएफ़पी के ब्लॉग पर प्रकाशित फ़ैक्ट-चेक में हम पाठकों को प्रत्येक स्टोरी का निष्कर्ष बताने के लिए एक रेटिंग देते हैं. रेटिंग या तो आर्टिकल में सबसे ऊपर हेडर इमेज का हिस्सा होती है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, या फिर फ़ैक्ट-चेक की शुरुआत में ही स्पष्ट होता है.

फ़ैक्ट-चेक की रेटिंग में हम निम्नलिखित टर्म्स का प्रयोग करते हैं:
- असत्य - इसमें हम यह कहते हैं कि ये दावा गलत है, जब कई तथ्य इसकी पुष्टि करते हैं.
- सत्य - इसमें हम यह कहते हैं कि ये दावा सही है, जब कई विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी के प्रामाणिक होने की पुष्टि होती है.
- भ्रामक - इसमें हम कहते हैं कि ये दावा भ्रामक है जब इसमें वास्तविक जानकारी (टेक्स्ट, फ़ोटो या वीडियो) को संदर्भ से अलग शेयर किया गया हो या गलत संदर्भ में एडिट किया गया हो.
- एडिटेड तस्वीर (आल्टर्ड इमेज) - जब धोखा देने या भ्रमित करने के लिए तस्वीर में हेरफ़ेर कर एडिट किया गया हो.
- आल्टर्ड वीडियो - जब धोखा देने या भ्रमित करने के लिए वीडियो में हेरफ़ेर किया गया हो.
- भ्रामक संदर्भ - जब किसी दावे में थोड़ी बहुत सत्यता हो लेकिन आगे की जानकारी के बिना वो दावा भ्रामक करने वाला हो सकता है.
- व्यंग्य - जब कोई दावा गलत हो और उसमें लोगों को गुमराह करने की क्षमता हो लेकिन मूल रूप से लोगों को भ्रमित करने का इरादा न हो (जैसे, हास्य, पैरोडी आदि).
- झांसा देना (होक्स) - जब कोई तस्वीर या घटना पूरी तरह से गढ़ी गई हो.
- डीप फ़ेक - जब किसी वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके हेरफ़ेर किया जाता है ताकि उसके वास्तविक प्रतीत होने जैसा एक बनावटी कंटेंट बनाया जा सके.
हमारी फ़ैक्ट-चेक प्रक्रिया और संपादकीय दिशानिर्देशों के बारे में अधिक जानकारी के लिये एएफ़पी की फ़ैक्ट-चेक शैलीपुस्तिका पढ़ सकते हैं.
ऑनलाइन प्लैटफ़ॉर्म्स के साथ हमारी साझेदारी
मेटा प्रोग्राम
फ़ेसबुक के थर्ड पार्टी फ़ैक्ट-चेक कार्यक्रम के सहभागी के रूप में हम फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर फ़्लैग/चिन्हित की गई पोस्ट को उस कंटेंट का हिस्सा मानते हैं जिसकी हम जांच करते हैं, और हमारे फ़ैक्ट-चेक बाद में उस पोस्ट पर दिखाई देते हैं जिसे हमने गलत, आंशिक रूप से गलत या भ्रामक संदर्भ के रूप में रेट किया होता है.
टिकटॉक प्रोग्राम
टिकटॉक के ग्लोबल फ़ैक्ट-चेकिंग प्रोग्राम के तहत हम टिकटॉक पर पोस्ट किए गए वीडियो को भी अपनी जांच का हिस्सा मानते हैं. हमारी फ़ैक्ट-चेकिंग टिकटॉक के इन-ऐप मॉडरेशन प्रक्रिया में भी योगदान देती है. इसके अलावा, हम अपनी वेबसाइट पर जो फ़ैक्ट-चेक प्रकाशित करते हैं, उनमें भी टिकटॉक पर मौजूद कंटेंट की जांच शामिल होती है.
व्हाट्सएप्प
ब्राज़ील, मेक्सिको, अमेरिका (स्पेनिश में), भारत, जर्मनी और फ़्रांस में काम कर रही हमारी फ़ैक्ट-चेकिंग टीमें व्हाट्सएप टिपलाइन संचालित करती हैं, जिसके माध्यम से जनता/यूज़र्स किसी भी भ्रामक या संदिग्ध दावे की जांच के लिए हमें पोस्ट भेज सकते हैं.
दावे की समीक्षा करने के टूल्स
एएफ़पी अपने फ़ैक्ट-चेक आर्टिकल में क्लेम रिव्यू टूल का उपयोग करता है. यह गूगल और बिंग जैसे सर्च इंजनों में किसी विशिष्ट दावे से जुड़ी खोज के रिप्लाई में आसानी से हमारी फ़ैक्ट-चेक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में मददगार साबित होता है.
हमारी साझेदारी और फ़ंडिंग के बारे में अधिक विवरण यहां पढ़ा जा सकता है.