
यह तस्वीर पाकिस्तान नहीं बल्कि 2014 में इराक में हुए बम धमाके की है
- यह आर्टिकल चार साल से अधिक पुराना है.
- प्रकाशित 1 सितम्बर 2021, 11h30
- 2 मिनट
- द्वारा AFP India
21 अगस्त को किये गए एक ट्वीट में लिखा गया, "पाकिस्तान में तालिबानियों की मदद से पहली मस्जिद अंतरिक्ष में लांच की गई बधाइयां रुकनी नहीं चाहिए."
ट्वीट में लगी तस्वीर में एक मस्जिद धुआं-धुआं होती दिख रही है.

यही तस्वीर ट्विटर पर यहां और यहां; और फ़ेसबुक पर यहां, यहां और यहां शेयर की गयी.
लेकिन यह दावा ग़लत है.
इस तस्वीर का गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें यह एक न्यूज़ रिपोर्ट में मिली जिसमें उत्तरी इराक के मोसुल में 2014 में हुए बम धमाके की जानकारी दी गयी है.
IraqiNews ने मोसुल में इस्लामिक स्टेट का मस्जिद पर हमले के बारे में 6 जुलाई, 2014 को अपनी एक रिपोर्ट में इस तस्वीर को प्रकाशित किया है.
ब्रिटिश अख़बार द इंडिपेंडेंट ने भी 14 जुलाई, 2014 को अपनी रिपोर्ट में ये तस्वीर छापते हुए कैप्शन लिखा है, "मोसुल के शिया अल-क़ुब्बा हुसैनिया मस्जिद में धमाका होते हुए." तस्वीर का क्रेडिट न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (AP) को दिया गया है.
नीचे भ्रामक ट्वीट (बाएं) और द इंडिपेंडेंट में छपी तस्वीर (दाएं) की तुलना में देख सकते हैं दोनों एक ही मौके की है.

इस बाबत कीवर्ड सर्च करने पर हफ़्फिंगटन पोस्ट की 7 जुलाई, 2014 की एक रिपोर्ट मिली जिसमें उसी मस्जिद में हुए धमाके की दूसरे एंगल से ली गयी तस्वीर है.
इस तस्वीर के साथ कैप्शन है, "ये तस्वीर बिना तारीख़ के एक मिलिटेंट वेबसाइट पर शेयर की गयी थी जो नियमित रूप से इस्लामिक स्टेट ग्रुप के बयान शेयर करता है. ये तस्वीर AP की इराक के मोसुल में शिया अल-क़ुब्बा हुसैनिया मस्जिद में धमाके पर रिपोर्टिंग से भी मेल खाती है."

यह तस्वीर AP के आर्काइव में मौजूद नहीं मिली.
AFP को पाकिस्तान में मस्जिद में तालिबान द्वारा किये गए ऐसे किसी भी धमाके की कोई न्यूज़ रिपोर्ट नहीं मिली.
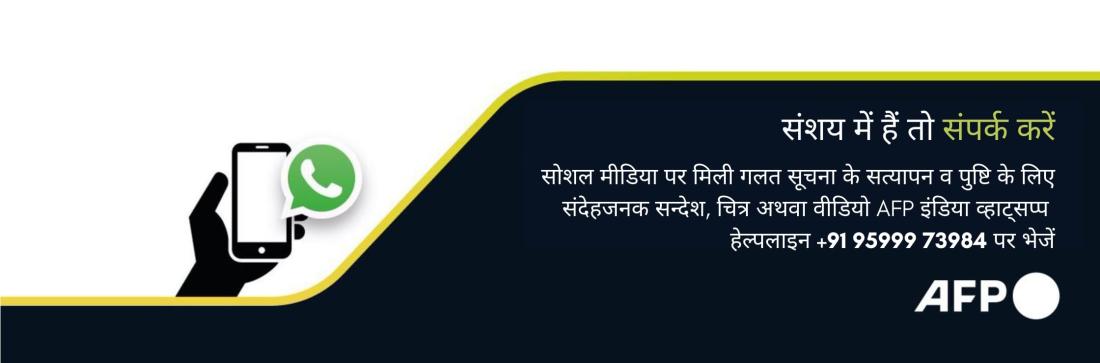
कॉपीराइट © एएफ़पी 2017-2025. इस कंटेंट के किसी भी तरह के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी. अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.



